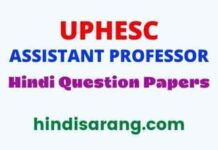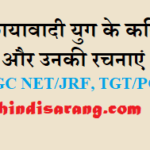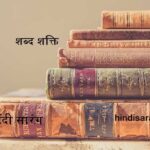उत्तर प्रदेश (UP) द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा (GDC Hindi) 2008 के प्रश्नपत्र का व्याख्यात्मक हल यहाँ दिया जा रहा है। GDC 2008 की इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा 2010 में आयोजित की गई थी। Print माध्यम से आप इस question papers pdf Download कर सकते हैं। यदि आप Higher Education संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देना चाहते हैं तो इसे जरुर पढ़ें। Assistant Professor हिंदी के दूसरे Exam और NTA UGC NET के लिए भी यह Question Papers महत्वपूर्ण है।
GDC Assistant Professor Hindi 2008
1. प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अन्तर है?
- प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बँधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना।
- प्रगतिवादी है मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी।
- प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना
- प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परम्पराओं का अनुपालन करना।
Ans (1): प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अन्तर यह है कि प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बँधे रहना है तथा प्रगतिशीलता जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना है।
प्रगतिवाद मार्क्सवाद विचारधारा से संबंधित है वहीं प्रगतिशीलता सापेक्ष स्थिति है। दोनों में अधिक अंतर नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य अपने आप में प्रगतिशील होता है। वहीं शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद के बारे में लिखा है कि, ‘प्रगतिवाद साहित्य की धारा ही नहीं साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है।’
2. एक दूसरे से भिन्न-भिन्न, नये-नये विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था-
- पहला तार सप्तक
- प्रथम तार सप्तक
- तार शप्तक
- तार सप्तक
Ans (4): एक दूसरे से भिन्न-भिन्न, नये-नये विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम ‘तार सप्तक’ था।
अज्ञेय के संपादकत्व में ‘तार सप्तक’ का प्रकाशन हुआ, इसी के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। उन्होने कुल 4 सप्तक का संपादन किया- तार सप्तक (1943), दूसरा सप्तक (1951), तीसरा सप्तक (1959) और चौथा सप्तक (1969)
तार सप्तक में निम्न कवि संकलित हैं- प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और अज्ञेय।
3. हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं-
- बंगला उपन्यास
- मराठी उपन्यास
- फ्रेंच उपन्यास
- अंग्रेज़ी उपन्यास
Ans (4): हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार ‘अंग्रेज़ी उपन्यास’ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ‘उपन्यास रहस्य’ निबंध में लिखा है कि उपन्यास का प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी है। बलकृष्ण भट्ट ने भी लिखा है कि ‘हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों कि नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं।’
4. ‘हिंदी कहानी का रचना विधान’ नामक कृति के प्रणेता हैं-
- डॉ. नगेंद्र
- नंददुलारे वाजपेयी
- जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
- डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्ण्य
Ans (3): ‘हिंदी कहानी का रचना विधान’ नामक आलोचनात्मक कृति के प्रणेता जगन्नाथ प्रसाद शर्मा हैं। ‘हिंदी गद्य शैली का विकास’ इनका अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
5. मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है-
- नहुष
- सिंदूर की होली
- रक्षाबंधन
- लहरों के राजहंस
Ans (4): मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक ‘लहरों के राजहंस’ है। इस नाटक की रचना मोहन राकेश ने वर्ष 1963 में किया था। ‘आषाढ़ का एक दिन’, ‘आधे अधूरे’, ‘पैरों तले जमीन’ नाटक तथा ‘अंडे के छिलके’ एकांकी इनकी अन्य रचनाएँ हैं।
6. हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है-
- कामना
- रजत शिखर
- आषाढ़ का एक दिन
- वत्सराज
Ans (1): हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक ‘कामना’ है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कन्दगुप्त, एक घूँट, चन्द्रगुप्त। ध्रुवस्वामिनी आदि उनके अन्य नाटक और एकांकी हैं।
7. ‘निबंध गद्य की कसौटी है।’ यह कथन है-
- बालकृष्ण भट्ट का
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
- प्रतापनारायण मिश्र का
- सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ का
Ans (2): ‘यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।’ यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
8. “कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यन्त भावुकताभरी रचनाएँ करने वाला जो रचनाकार अपने ‘रेखाचित्रों में अत्यन्त स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है-
- जयशंकर प्रसाद
- महादेवी वर्मा
- रामवृक्ष बेनीपुरी
- विष्णु प्रभाकर
Ans (2): कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यन्त भावुकताभरी रचनाएँ करने वाला जो रचनाकार अपने ‘रेखाचित्रों’ में अत्यन्त स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम ‘महादेवी वर्मा’ है।
महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री रही हैं। इसीलिए उनके रहस्यवाद को दार्शनिक रहस्यवाद कहा जाता है। महादेवी के प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। निहार, रश्मि, निरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि उनकी काव्य कृतियाँ हैं।
9. भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा-दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं?
- डॉ. महावीर प्रसाद द्विवेदी
- नंददुलारे वाजपेयी
- गजानन माधव मुक्तिबोध
- रामचंद्र शुक्ल
Ans (4): भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा-दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक ‘रामचंद्र शुक्ल’ हैं।
10. ‘रसमीमांसा’ नामक शास्त्रीय समीक्षा-दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं?
- डॉ. नगेंद्र
- नंददुलारे वाजपेयी
- भागीरथ मिश्र
- रामचंद्र शुक्ल
Ans (4): ‘रसमीमांसा’ नामक शास्त्रीय समीक्षा-दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक ‘रामचंद्र शुक्ल’ हैं। यह शुक्लजी का सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है। सूर, तुलसी, जायसी, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि उनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
11. निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएँ जो समालोचक के साथ-साथ जनवादी कवि भी हैं–
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
- डॉ. निर्मला जैन
- डॉ. रामविलास शर्मा
- डॉ. विजयेन्द्र स्नातक
Ans (3): डॉ. रामविलास शर्मा समालोचक के साथ-साथ जनवादी कवि भी थे। प्रेमचंद, भारतेन्दु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिंदी आलोचना आदि उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
12. ‘कामायनी एक पुनर्विचार’ नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ लेखक हैं-
- नंददुलारे वाजपेयी
- डॉ. रामविलास शर्मा
- हजारी प्रसाद द्विवेदी
- मुक्तिबोध
Ans (4): ‘कामायनी एक पुनर्विचार’ नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ लेखक ‘मुक्तिबोध’ हैं। ‘नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध’ तथा ‘नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र’ उनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
13. “उचित चेति च्यंति लै ताही।” -पदांश में प्रयुक्त ‘च्यंति’ शब्द बाबू श्यामसुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह शब्द ‘च्यंति’?
- चित्त लेटने का
- चितवन को
- सोच-विचार करने का
- चेतना के स्तर को प्रकट करने को
Ans (4): ‘उचित चेति च्यंति लै ताही’ पदांश में प्रयुक्त ‘च्यंति’ शब्द बाबू श्यामसुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति चेतना के स्तर को प्रकट करने को प्रकट करने वाला है।
14. “कबीर का गर्व और दैन्य, दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं।” -यह कथन है-
- पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी का
- डॉ. माताप्रसाद गुप्त का
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
- बाबू श्यामसुंदर दास का
Ans (1): “कबीर का गर्व और दैन्य, दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं।” -यह कथन पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जिसे उन्होंने कबीर के विषय में कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को ‘भाषा का डिक्टेटर’ भी कहा है। वहीं श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा है।
15. ‘बल्लभाचार्य’ जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं-
- रूद्र
- ब्रह्म
- सनकादि
- श्री
Ans (1): ‘बल्लभाचार्य’ रूद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, जिसके प्रवर्तक ‘विष्णुस्वामी’ हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, शृंगाररस मंडन, विद्वमंडन आदि उनके ग्रंथ हैं।
16. ‘श्रीकृष्ण-भक्ति’ शाखा में मधुरा-भक्ति-भावना का समावेश हुआ, निम्नलिखित के अनुकरण में-
- मलिक मुहम्मद जायसी
- चैतन्य महाप्रभु
- स्वामी हरिदास
- रसखान
Ans (2): ‘श्रीकृष्ण-भक्ति’ शाखा में मधुरा-भक्ति-भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। इन्होंने ‘गौंडीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया था तथा इनका दार्शनिक मत ‘अचिंत्य भेदाभेदवाद है।
17. “संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियौ।
कलि-कुटिल जीव निस्तार हित, बालमीकि तुलसी भयौ।”
-यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है?
- रहीम
- स्वामी अग्रदास
- नाभादास
- रामानंद
Ans (3): उपरोक्त उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने वर्ष 1592 ई. में भक्तमाल की रचना किया था जिसमें 200 पुराने एवं नये भक्तों का चरितगान (चमत्कारपूर्ण चरित्र) ब्रजभाषा में तथा 316 छप्पयों में लिखा गया है।
18. ‘खालिक बारी’ किसकी रचना है?
- अमीर खुसरो
- निजामुद्दीन औलिया
- मलिक मुहम्मद जायसी
- नूरमुहम्मद
Ans (1): ‘खालिक बारी’ अमीर खुसरो की रचना है जो अरबी, फारसी और हिंदी का कोश है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को ‘तोता-ए-हिंद’ की उपाधि दी थी। ‘तुर्क-ए-अल्लाह’ इनका उपनाम है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन काल देखा था।
19. सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण- “नखत वेद ग्रह जोरि अरध करि को बरजै हम खात।” से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है?
- अमृत
- खीर
- विष
- कल्पवृक्ष का फल
Ans (3): सूरदास के उपरोक्त पद से ‘विष’ खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है।
“नखत वेद ग्रह जोरि अरध करि को बरजै हम खात।” अर्थात 27 नक्षत्र + 4 वेद + 9 ग्रह= 40 / 2 = 20 होता है, जहाँ 20 का अभिप्राय ‘विष’ से है।
20. ‘रसखान’ कवि का वास्तविक नाम था-
- नसीमखान
- अली मुहम्मद
- अब्दुल
- सैयद इब्राहीम
Ans (4): ‘रसखान’ कवि का वास्तविक नाम ‘सैयद इब्राहीम’ था। सरल, ह्रदयग्राही और रसपूर्ण भाषा प्रयोग के कारण रसखान को ‘पीयूषवर्णी’ अथवा ‘अमृत का वर्षा करने वाला कवि’ कहा गया है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं हुआ। भारतेंदु ने लिखा है कि, ‘इन मुसलमान हरिजन पै, कोटिक हिंदू वारिए।’ प्रेमवाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दानलीला आदि इनकी रचनाएँ हैं।
21. ‘अष्टछाप’ की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की?
- बिट्ठलदास जी ने
- बल्लभाचार्य जी ने
- उपर्युक्त दोनों ने
- इनमें से किसी ने नहीं
Ans (1): ‘अष्टछाप’ की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा बिट्ठलदास जी ने की थी। गुसाई बिट्ठलनाथ ने 1565 ई. में अपने पिता बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 प्रधान शिष्यों को लेकर संगीतज्ञों की एक टोली का निर्माण किया था जो ‘अष्टछाप’ या ‘अष्टसखा’ के नाम से जाने जाते हैं। अष्टछाप में निम्नलिखित कवि शामिल थे-
बल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंददास तथा गुसाई बिट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंदस्वामी, छीतस्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास।
22. “कमल दल नैनन की उनमानि।
बिसरत नाहि सखी मो मन तें मंद-मंद मुसकानि।”
-यह पद चरण किसकी रचना है?
- मीराबाई
- रहीम
- सूरदास
- नंददास
Ans (2): यह पद चरण रहीम की रचना है। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। इनका पूरा नाम अब्दुर्रहीम खानखाना था। ये दानवीर थे इसीलिए दानशीलता में इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। रहीम बरवै छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। बरवै नायिका भेद, बरवै, नगर शोभा, मदनाष्टक, शृंगार सोरठा, खेट कौतुकम्, दोहवाली या सतसई आदि इनकी रचनाएँ हैं।
23. “बरसे मघा झकोरि-झकोरी। मोर दुइ नैन चुवैं जस ओरी।” इस अर्द्धाली में आए ‘ओरी’ शब्द का अर्थ है-
- अरे ओ सखी री, मेरे आँसुओं को देखो।
- जिसका ओर-छोर न हो, ऐसी लगातार बारिश।
- ओरा जाना, समाप्त हो जाना।
- छाजन से गिरनेवाली पानी की धार।
Ans (4): उपरोक्त अर्द्धाली में आए ‘ओरी’ शब्द का अर्थ ‘छाजन से गिरनेवाली पानी की धार’ है। उपरोक्त पंक्ति जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के बारहमासा से लिया गया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि इनकी रचनाएँ हैं।
24. “पंडित और प्रबीनन कौ जोइ चित्त हरै, सो कवित्त कहावै।”
-यह किस कवि का कथन है?
- बिहारी
- घनानंद
- ठाकुर
- देव
Ans (3): उपरोक्त कथन ठाकुर का है। इनके आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केशरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक आदि इनकी रचनाएँ हैं।
25. “लिखन बैठि जाकी, सबी, गहि-गहि गरब गरूर।
भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर”
-उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएँ कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि (पोट्रेट) को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे?
- चित्रकारों की आँखें चौंधिया जाती थीं।
- चित्र बनाकर जब मिलाया, तब तक रूप नये स्वरूप में बदल गया।
- घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे।
- चित्रकार बैठ कर चित्र बनाते थे, जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे।
Ans (2): उपरोक्त दोहे में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया, तब तक रूप नये स्वरूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे।
26. “छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया।” इस संदर्भ में कौन-सा विकल्प सही है-
- बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया।
- बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किये बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके।
- हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। कर
- बंगला साहित्य में छायावाद-युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे।
Ans (4): “छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया।” इस संदर्भ में ‘बंगला साहित्य में छायावाद-युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे।’ कथन सही है।
27. “पुरातनता का यह निर्मोक
सहन-करती न प्रकृति पल एक”
-यहाँ ‘निर्मोक’ से अभिप्राय है?
- साँप के शरीर पर लिपटी कँचुली
- निष्ठुर आघात
- नितान्त अनावश्यक भार
- निकम्मापन
Ans (1): यहाँ ‘निर्मोक’ से अभिप्राय ‘साँप के शरीर पर लिपटी कँचुली’ से है। उपरोक्त कथन जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा हताश मनु से कहती है।
28. “विकल-वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए।” -यहाँ ‘वे’ से तात्पर्य है?
- सुरा-सुरभिमय लालिमा युक्त मुख-मण्डल
- देव सृष्टि के अहंकारी देवगण
- कामवासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल-चरित्र
- स्त्रियों के क्वणित कंकण के, केशर-कुंकुमित वक्ष स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्य गण
Ans (2): “विकंल-वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए।” -यहाँ ‘वे’ से तात्पर्य ‘देव सृष्टि के अहंकारी देवगण’ है। उक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत ‘कामायनी’ महाकाव्य की है।
29. “मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान”
उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गयी है। ऐसा संभव होने का आधार है-
- भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है।
- भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुला कर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है।
- अस्तित्व ज्ञान भुला कर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुँचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है।
- अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है।
Ans (3): उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गयी है। ऐसा संभव होने का आधार है- अस्तित्व ज्ञान भुला कर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुँचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की ‘नौका विहार’ कविता की है। जिसमें पंत ने नौका विहार की तुलना जीवन के शाश्वत रूप से की है।
30. “लख महा भाव-मंगल पद तल धँस रहा गर्व-मानव के मन का असुर मन्द हो रहा खर्चा।”
इन काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है, उसका आधार है-
- मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली।
- पैरों तले रौंदने पर ही घमंडी के वश में आने की प्रवृत्ति।
- ब्रह्म प्रकृति में अन्त प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली।
- बंगाली संस्कृति में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली।
Ans (1): इन काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है, उसका आधार मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की ‘अनामिका’ काव्य संग्रह की है।
31. “अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान?”
मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन: स्थिति का द्योतक है?
- असहायता
- भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति।
- कभी पूरा न करने की लाचारी।
- राक्षसी-वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता।
Ans (2): मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन ‘भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति’ विशेष का मन: स्थिति का द्योतक है। यह पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की ‘ब्रह्म राक्षस’ कविता की है। मुक्तिबोध ने इस कविता में ब्रह्म राक्षस मिथक के द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव को चित्रित किया है। यह पंक्ति नागार्जुन की ‘बादल को घिरते देखा है’ कविता की है।
32. “निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो-हो कर” वक्तव्य का तात्पर्य है-
- अपने से बेगाना हो जाना।
- मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना।
- पगलाए फिरते रहना।
- अपनी ही अन्तशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना।
Ans (4): “निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो-हो कर” वक्तव्य का तात्पर्य है- अपनी ही अन्तशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना।
33. ‘कामायनी’ की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि-
- जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे।
- उस कोटि की रचना का शीर्ष-शिखर ‘कामायनी’ हो चुकी थी।
- अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प-कौशल के आगे हार मान चुके थे।
- कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था।
Ans (2): ‘कामायनी’ की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष-शिखर ‘कामायनी’ हो चुकी थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का फैन्टेसी युक्त कल्पना प्रधान महाकाव्य है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमश: मानव, प्रेम और बुद्धि के प्रतीक हैं।
34. “यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है।” -यह कथन किसका है?
- आचार्य नंददुलारे वाजपेयी
- डॉ. नगेंद्र
- जयशंकर प्रसाद
- मुक्तिबोध
Ans (3): उपरोक्त कथन जयशंकर प्रसाद का है।
कामायनी के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के कथन-
- जयशंकर प्रसाद- यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है।
- आचार्य नंददुलारे वाजपेयी- कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है।
- मुक्तिबोध- कामायनी जीवन की पुनर्रचना है।
- डॉ. नगेंद्र- कामायनी समग्रत: में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है।
- हजारी प्रसाद द्विवेदी- कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है।
35. प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यन्त्र क्यों नहीं मिलता?
- प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका।
- पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था, वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया।
- प्रकृति-चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है।
- प्रकृति-चित्रण में कथावस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना।
Ans (1): प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यन्त्र
इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका।
36. “मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं।” -यह किस विद्वान् का कथन है?
- डॉ. रामविलास शर्मा
- प्रभाकर माचवे
- नागार्जुन
- शमशेर बहादुर सिंह
Ans (4): उपरोक्त कथन शमशेर बहादुर सिंह का है।
‘अंधेरे में’ (मुक्तिबोध) कविता के विषय में विद्वानों के कथन-
- प्रभाकर माचवे- इसके (अंधेरे में) बहुत से अंश पिकासो के विश्वप्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते हैं।
- डॉ. रामविलास शर्मा- अपराध भावना का अनुसंधान & आरक्षित जीवन की कविता
- नामवर सिंह- अस्मिता की खोज
37. नागार्जुन की जनवादी छवि “सैनिक-कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है।” यह कथन है-
- केदारनाथ सिंह का
- रामविलास शर्मा का
- अज्ञेय का
- डॉ. कशेरी कुमार का
Ans (2): उपरोक्त कथन रामविलास शर्मा का है। वहीं नामवर सिंह के अनुसार, ‘इस बात में तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले एसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुँच किसानों की चौपालों से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है।
38. “काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अन्त में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि-मर्म इसी परिभाषा से नि:सृत होते हैं।”
अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय है कि-
- मात्र शब्द की साधना में सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है।
- शब्दकीड़ा की योजना ही कवि का काम है।
- श्रेष्ठ साहित्य मूलत: शब्दज्ञान पर निर्भर होता है। अतः सब छोड़कर शब्द को ही सँवारना उचित है।
- शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि-मर्म सफल हो जाता है।
Ans (4): अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय है कि- शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि-मर्म सफल हो जाता है।
39. ‘छायावाद’ को समग्र रूप से समझने-समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं-
- रामचंद्र शुक्ल
- पं. नलिन विलोचन शर्मा
- नंददुलारे वाजपेयी
- डॉ. नगेंद्र
Ans (3): ‘छायावाद’ को समग्र रूप से समझने-समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंददुलारे वाजपेयी हैं।
40. “दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश।” किस काव्य-कृति का प्रबोध वाक्य है?
- पल्लव
- राम की शक्ति पूजा
- चाँद का मुँह टेढ़ा है
- कामायनी
Ans (4): “दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश।” यह कामायनी काव्य-कृति का प्रबोध वाक्य है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में 15 सर्ग निम्न हैं- चिंता, आशा, श्रधा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
41. लोक-मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है?
- जायसी
- तुलसीदास
- अज्ञेय
- मुक्तिबोध
Ans (2): लोक-मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास कृत रामचरित मानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है।
जार्जग्रियर्सन- महात्मा बुध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास।
हजारी प्रसाद द्विवेदी- लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके।
42. बाल-वर्णन संबंधी कविताएँ आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल-वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है?
- द्वारका प्रसाद महेश्वरी
- सुमित्रानंदन पंत
- सूरदास
- बिहारी
Ans (3): समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल-वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। सूरदास ने वात्सल्य रस का जैसा मनोमुग्धकारी वर्णन किसी और के यहाँ नहीं मिलता।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल- वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। …इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी- सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और बालक ह्रदय लेकर ही इस संसार का निबाह कर गये।
43. भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है-
- व्यक्तित्व का परिशोधन
- चरित्र-चित्रण
- दृश्यों का प्रस्तुतीकरण
- रसास्वादन
Ans (4): भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है।
44. ‘चंद्रावली नाटिका’ के रचयिता हैं-
- जयशंकर प्रसाद
- धर्मवीर भारती
- भारतेंदु हरिशचंद्र
- हरिकृष्ण भारती
Ans (3): ‘चंद्रावली नाटिका’ के रचयिता भारतेंदु हरिशचंद्र हैं। यह भारतेंदु का मौलिक नाटक है जिसमें वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण हुआ है।
भारतेंदु के मौलिक नाटक- वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम्, प्रेमजोगिनी, चंद्रावली, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप।
45. ‘प्रसाद’ के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं?
- नंददुलारे वाजपेयी
- लक्ष्मी नारायण लाल
- डॉ. दशरथ ओझा
- डॉ. धीरेंद्र वर्मा
Ans (1): ‘प्रसाद’ के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंददुलारे वाजपेयी हैं। नंददुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य: सृजन और समीक्षा, नया साहित्य नये प्रश्न आदि उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
46. “अपने कुकर्मों का फल चखने में कडुआ, परन्तु परिणाम में मधुर होता है।” यह कथन है-
- स्कंदगुप्त
- प्रख्यातिकीर्ति
- मातृगुप्त
- भटार्क
Ans (4): यह कथन प्रसाद के नाटक स्कन्दगुप्त के पात्र भटार्क का है। कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त, पृथ्वीसेन, वन्धुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देव-सेना, विजया आदि स्कन्दगुप्त नाटक के अन्य पात्र हैं।
47. “मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है। जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं।”
यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है?
- भारत दुर्दशा
- अंधेरनगरी
- चंद्रगुप्त मौर्य
- स्कंदगुप्त
Ans (4): उपरोक्त संवाद जयशंकर प्रसाद के स्कन्दगुप्त नाटक का है।
48. ‘भारत-दुर्दशा’ नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था-
- भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना।
- अंग्रेजी-शासन की व्याजस्तुति करना।
- भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अन्यान्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है।
Ans (3): ‘भारत-दुर्दशा’ नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस हास्य रूपक के माध्यम से प्रसाद ने भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की निंदा की है।
49. अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी-
- ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग।
- रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना।
- नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य-पद्य में करना।
- हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग देना।
Ans (2): अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना था। भारतेंदु युग में सर्वाधिक विकास नाटक विधा का हुआ जिसका श्रेय भारतेंदु को ही जाता है।
50. “एक जमाने में नाटकों के असंभव समझें जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषत: उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि-
- दृश्य बहुत जल्दी-जल्दी बदलने पड़ते हैं।
- पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है।
- नाटक देखनेवाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुँच पायी।
- अभिनेताओं-अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साजपोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता।
Ans (3): “एक जमाने में नाटकों के असंभव समझें जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषत: उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि- नाटक देखनेवाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुँच पायी।
51. आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं?
- व्यक्तिव्यंजक
- चरित्रचित्रणात्मक
- संभाषणात्मक
- वस्तुव्यंजक
Ans (4): आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तुव्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं।
52. हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएँ हो रही थीं, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ठ काव्यकृति थी-
- पल्लव
- साकेत
- जौहर
- परिमल
Ans (1): हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएँ हो रही थीं, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ठ काव्यकृति ‘पल्लव’ थी। पल्लव को छायावाद का घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) और प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पंत ने पल्लव की भूमिका के माध्यम से छायावादी विरोधियों का मुँह बंद बंद करने का प्रयास किया।
53. ‘गोदान’ उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है?
- मिस्टर खन्ना
- मिर्जा खुर्शेद
- ओंकारनाथ
- मेहता
Ans (4): ‘गोदान’ उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता हैं। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, रायसाहब, मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन, गोविंदी आदि इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं।
54. ‘गोदान’ उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है-
- बहुत कम-चरित्रों को शामिल करने से।
- शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से।
- दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लम्बे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से।
- साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से।
Ans (2): ‘गोदान’ उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से कमी आई है।
55. “आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है।”
-यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है?
- स्कंदगुप्त
- चिंतामणि
- दिव्या
- गोदान
Ans (3): उपरोक्त पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है।
56. यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूँस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है-
- फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद
- सार्त्र का अस्तित्ववाद
- मार्क्स-लेनिन का साम्यवाद
- महर्षि अरविंद का दर्शन
Ans (3): यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूँस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स-लेनिन का साम्यवाद।
57. ‘मैला आँचल’ की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह-जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि-
- इसमें ग्रामीण और शहरी, दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है।
- परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है।
- लोक-कथाओं, लोकोक्तियाँ, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है।
- इसमें व्याकरणजन्य त्रुटियाँ नहीं है।
Ans (2): ‘मैला आँचल’ की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह-जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। ‘मैला आँचल’ फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है जिसमें उन्होंने नेपाल सीमा से सटे उत्तर-पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर जिवंत और मुखर चित्रण किया है।
58. “बावन ने दो आजाद देशों की-हिंदुस्तान और पाकिस्तान की-ईमानदारी को, इंसानियत को, बस दो डग में नाप लिया।” यह कथन है-
- सुमिरत दास का
- पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का
- फणीश्वरनाथ रेणु का
- डॉ. प्रशांत का
Ans (3): उपरोक्त कथन फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आँचल उपन्यास का है। 1954 ई. में प्रकाशित इस उपन्यास की कथावस्तु उत्तर-पूर्वी विहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव की है।
59. “कितने ही सिद्धांत, जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएँ आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है।”
-यह निम्नलिखित में से किसका कथन है?
- प्रेमचंद
- रामचंद्र शुक्ल
- अज्ञेय
- जैनेंद्र
Ans (1): यह कथन प्रेमचंद (गोदान उपन्यास) का है।
60. “लड़कपन था, तब मैं उसके समकक्ष था। हममें कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है। मैं छोटा हो गया हूँ।”
-यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है?
- ईदगाह
- अलग्योझा
- शतरंज के खिलाड़ी
- गुल्लीडंडा
Ans (4): यह प्रेमचंद द्वारा रचित ‘गुल्ली-डंडा’ कहानी का अंश है।
61. निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था?
- कमलेश्वर
- ममता कालिया
- जैनेंद्र
- हरिशंकर परसाई
Ans (3): जैनेंद्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। फाँसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राज कन्या, ध्रुवयात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि उनके कहानी संग्रह हैं।
62. प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल-चरित्र का अनोखा वर्णन है?
- शतरंज के खिलाड़ी
- कफन
- सभ्यता का रहस्य
- ईदगाह
Ans (4): प्रेमचंद जी के ईदगाह कहानी में बाल-चरित्र का अनोखा वर्णन है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान को बड़े ही मनोयोग से उकेरा है।
63. साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि-
- इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता।
- शासन-सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है।
- जीवधारी राजपुरूषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है।
- देश-विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर, उनकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है।
Ans (3): साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि देश-विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर, उनकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है।
64. भारतीय साहित्यशास्त्र में रस-निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार्य की स्थापना है–
- आनंदवर्धन
- आचार्य भरत
- भट्टनायक
- पंडितराज जगन्नाथ
Ans (2): भारतीय साहित्यशास्त्र में रस-निष्पत्ति सिद्धांत आचार्य भरत नामक साहित्याचार्य की स्थापना है। नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस की निम्न परिभाषा दी है- विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पति:।
65. मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है?
- हरियाणवी
- मराठी की
- राजस्थानी की
- पंजाबी की
Ans (3): मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं और इनकी उपासना माधुर्य भाव की है। इनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरां की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि इनकी रचनाएँ हैं।
66. कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य-विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है?
- रामचंद्रिका
- कविप्रिया
- रसिकप्रिया
- रतन बावनी
Ans (1): कवि केशवदास की रामचंद्रिका अपने वर्ण्य-विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यह एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका में केशवदास को ‘संवाद योजना’ में बेजोड़ सफलता हाँथ लगी है।
- रामस्वरूप चतुर्वेदी- छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायबघर है।
- डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल- रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है।
67. “भरि रही भनक बनक ताल तालन की।
तनक-तनक तामें खनक चुरीन की।”
-ये किस कवि के छंद की पंक्तियाँ है?
- रत्नाकर
- पद्माकर
- देव
- द्विजदेव
Ans (3): उपरोक्त पंक्तियाँ कवि देव की हैं।
68. आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है-
- मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना।
- गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना।
- नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना।
- भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना।
Ans (2): आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है।
69. वे कवि जो काव्य-सर्जना के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रगण्य हैं–
- अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
- मुकुटधर पांडेय
- मैथिलीशरण गुप्त
- रूपनारायण पांडेय
Ans (3): वे कवि जो काव्य-सर्जना के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रगण्य मैथिलीशरण गुप्त हैं। मैथिलीशरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ‘साकेत’ है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी और हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है।
70. किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है-
- संस्मरण
- आत्मकथा
- फीचर
- रेखाचित्र
Ans (4): किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखाचित्र है। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्कैच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा (1937 ई.) हिंदी का पहला रेखाचित्र है।
71. प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं?
- सुमित्रानंदन पंत
- गजानन माधव मुक्तिबोध
- भगवती चरण वर्मा
- रामधारी सिंह दिनकर
Ans (2): प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और ‘तीब्र इन्द्रियबोध’ का कवि कहा जाता है। चाँद का मुँह टेढ़ा है और भूरि भूरि खाक धूलि इनके काव्य संग्रह हैं।
72. नयी-नयी काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं-
- नेमिचंद्र जैन
- गिरिजाकुमार माथुर
- धर्मवीर भारती
- अज्ञेय
Ans (4): नयी-नयी काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं।
73. भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है-
- भाषा मानव-मुख के ध्वन्यंगों से नि:सृत, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार-विनिमय का माध्यम है।
- प्राणियों के पारस्परिक विचार-विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो।
- सभ्य-समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो।
- बोलने-चालने, पढ़ने-लिखने, शिक्षण-प्रशिक्षण, कार्यालयीय, न्यायालयीय व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो।
Ans (1): भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है- भाषा मानव-मुख के ध्वन्यंगों से नि:सृत, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार-विनिमय का माध्यम है।
- कामता प्रसाद गुरु- भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, दूसरों पर भली-भांति प्रगट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है।
- डॉ. श्यामसुंदर दास- विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं।
74. भाषा की लघुत्तम इकाई है-
- ध्वनि
- पद
- वाक्य
- अर्थ
Ans (1): भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण भी कहा जाता है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और जब कोई सार्थक शब्द वाकया में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं।
75. ‘पालि’ पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है-
- प्राकृत > पाकट > पाअड > पाउल > पालि
- पंक्ति > पन्ति > पट्टि > पल्लि > पालि
- परियाय > पलियाय > पालियालि > पालि
- पाठ > पाट्टि > पाल्लि > पालि
Ans (3): ‘पालि’ पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है- परियाय > पलियाय > पालियालि > पालि। यह व्युत्पति भाषा विद्वान् भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी है। त्रिपिटक की भाषा पालि है इसीलिए इसे ‘बुध वचन’ भी कहा गया है।
76. पालि भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है-
- काच्चायन
- पंतजलि
- पाणिनि
- हेमचंद्र
Ans (1): पालि भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण काच्चायन हैं। पालि भाषा के तीन व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं-
- कच्चायन व्याकरण- महा काच्चायन
- मोग्गलान व्याकरण- मोग्गलान
- सद्दनीति व्याकरण- बर्मी भिक्षु अग्गवंश
77. “प्रकृति संस्कृतम् तदागतम् प्राकृतम” उक्ति का उचित भावार्थ है-
- प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई।
- प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत उससे जो विकसित हुई, यह प्राकृत भाषा कहलाई।
- प्रकृति भाषा को माँज कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक-व्यवहार में घिसते-घिसते वह प्राकृत भाषा हो गई।
- भाषा की प्रकृति है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु वह जब संस्कार-विहीन हो जाती है, तब प्राकृत भाषा रूप में रह जाती है।
Ans (2): “प्रकृति संस्कृतम् तदागतम् प्राकृतम” उक्ति का उचित भावार्थ है- प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत उससे जो विकसित हुई, यह प्राकृत भाषा कहलाई।
प्राकृत-वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि (7वीं शताब्दी) का आता है। इनका व्याकरण ग्रंथ ‘प्राकृत प्रकाश’ है जिसमें प्राकृत के चार भेद बताया गया है- महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौरसेनी। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है।
78. अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ-
- संस्कृत भाषा से
- पालि भाषा से
- दरद भाषा से
- प्राकृत भाषाओं से
Ans (4): अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं से हुआ। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है इसलिए इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है।
अपभ्रंश भाषा का विकास निम्न रूप में हुआ-
संस्कृत- पालि- प्रकृति- अपभ्रंश- अवहट्ठ- हिंदी
79. हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप विकसित हुआ न देख, उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया ‘पुरानी हिंदी’-
- आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा
- डॉ. बाबूराम सक्सेना
- चंद्रधर शर्मा गुलेरी
- सर जार्ज ऐब्राहम ग्रियर्सन
Ans (3): हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप विकसित हुआ न देख, उसके एक विशेष युगीन रूप को भाषाविद चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ‘पुरानी हिंदी’ नाम दिया।
80. गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है?
- निर्गुण भक्त कवि
- पुरानी हिंदी के कवि
- प्राकृत काल के कवि
- बौद्ध-तांत्रिक सिद्ध कवि
Ans (2): गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन्हें नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। सबदी, पद, प्राण-सांकली, शिष्य दर्शन, नरवें बोध, सप्तावर, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञानतिलक, ज्ञानचौंतीसा, अभयमात्र जोग, पंचमात्रा, गोरखबोध आदि गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था।
81. हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ–
- ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन-सत्ता का एक मात्र केंद्र था।
- उस समय की सभी भाषाओं से ब्रजभाषा ही सबसे अधिक संबद्ध थी।
- ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा-भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया।
- ब्रजभाषा-भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए थे।
Ans (3): हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा-भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। साहित्यिक ब्रजभाषा 10वीं-11वीं शताब्दी के आस-पास ही शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई।
82. अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है-
- मलिक मुहम्मद जायसी को
- कुतुबन को
- गोस्वामी तुलसीदास को
- अमीर खुसरो को
Ans (3): अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओँ में रचनाएँ की हैं-
- अवधी भाषा में रचित ग्रंथ- रामचरित मानस, पार्वतीमंगल, जानकी मंगल, रामलाला नहछू, बरवै रामायण
- ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ- विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञाप्रश्न, श्रीकृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक आदि।
83. खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरम्भ हुआ-
- बोल-चाल में अत्यधिक व्यवहार करने से।
- हिंदी पद्यबद्व रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा-टीकाओं से।
- बंगला रचनाओं तथा अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से।
- महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएँ करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से।
Ans (4): खड़ी बोली गद्य का विकास महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएँ करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से आरम्भ हुआ। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को काव्यभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित किया था।
84. खड़ी बोली गद्य के-विकास का मूल आधार बना-
- इसका कलकत्ता तक फैल जाना।
- फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना।
- हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना।
- खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना।
Ans (4): खड़ी बोली गद्य के-विकास का मूल आधार खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना बना।
खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना अकबर के दरबारी कवि गंग की ‘चंद छंद बरनन की महिमा’ है, जिसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम रामप्रसाद निरंजनी द्वारा रचित ‘भाषायोगवशिष्ठ’ में मिलता है।
85. भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई-
- 10 मई सन् 1963 ई. को
- 15 अगस्त सन 1947 ई. को
- 26 जनवरी सन् 1950 ई. को
- 14 सितम्बर सन् 1949 ई. को
Ans (4): भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितम्बर सन् 1949 ई. को प्राप्त हुई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को ही ‘हिंदी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 (1) में किया गया है- “संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।”
86. हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे-
- पं. जवाहरलाल नेहरू
- राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन
- राजगोपालचारी
- श्री गोपालस्वामी आयंगार
Ans (4): हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक श्री गोपालस्वामी आयंगार थे। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओँ को मान्यता प्रदान की गई है।
87. वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है?
- राष्ट्रभाषा
- संचार भाषा
- माध्यम भाषा
- राजभाषा
Ans (4): वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
88. राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है-
- जो पूरे राष्ट्र में पायी जाती है।
- राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था (संसद) जिसे मान्यता प्रदान करती है।
- विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं।
- राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भण्डार सबसे अधिक समृद्ध होता है।
Ans (1): राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है, जो पूरे राष्ट्र में पायी जाती है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है अर्थात आमजन भाषा (जनभाषा) है।
89. मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है, जिससे-
- उस भाषा का सम्मान बढ़ता है।
- भिन्न-भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है।
- जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जाँची-परखी जाती है।
- प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है।
Ans (2): मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है, जिससे भिन्न-भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है।
90. भारतीय भाषाओं के भाषा-सर्वेक्षण का कार्य-संपादन एवम् कई खण्डों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ-
- टी.एस. तोसीतोरी
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल
- सुनीति कुमार चटर्जी
- सर जॉर्ज ऐब्राहम ग्रियर्सन
Ans (4): भारतीय भाषाओं के भाषा-सर्वेक्षण का कार्य-संपादन एवम् कई खण्डों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज ऐब्राहम ग्रियर्सन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जार्ज ग्रियर्सन ने ‘दि मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान’ (1888 ई. में) नाम से फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ भी लिखा है।
91. हिंदी की वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है-
- केंद्रीय हिंदी संस्थान
- केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
- राजभाषा अनुभाग
Ans (3): हिंदी की वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। यह संस्था हिंदी और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करती है। इसकी स्थापना 1950 ई. में शिक्षा संस्था द्वारा की गई थी। 1960 ई. में में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय और 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनिकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई।
92. हिंदी की वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं-
- हिंदी भाषा से
- मराठी भाषा से
- बंगला भाषा से
- सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से
Ans (4): हिंदी की वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं।
93. कुमायूँनी भाषा-भाषी क्षेत्र है-
- जम्मू क॒श्मीर-हिमाचल प्रदेश
- रानीखेत-नैनीताल
- कुरक्षेत्र-अंबाला-हिसार
- लखीमपुर-खीरी-पीलीभीत-शाहजहाँपुर
Ans (2): कुमायूँनी भाषा-भाषी क्षेत्र उत्तराखंड का रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौड़गढ़, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर आदि है। कुमायूँनी पहाड़ी हिंदी की बोली है।
94. भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढाँचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है–
- बंगला भाषा से
- फारसी भाषा से
- ब्रजभाषा से
- बुंदेली भाषा से
Ans (1): भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढाँचे में बंगला भाषा से काफी समानता रखती है। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। भोजपुर, शाहाबाद, सारन, छपरा, चंपारण, राँची, जशपुर, पलामू का कुछ भाग आदि बिहार के और वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि उत्तर प्रदेश के जिलों में भोजपुरी बोली जाती है।
95. खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा-भाषी क्षेत्र है-
- मेरठ-बुलंदशहर-खुर्जा
- रोहतक-गुड़गाँव-फरीदाबाद
- पानीपत-कुरुक्षेत्र-अंबाला
- इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं
Ans (1): खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा-भाषी क्षेत्र मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा है। यह बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर, मुरादाबाद आदि जिलों में बोली जाती हैं।
96. ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है-
- महाराष्ट्री अपभ्रंश
- शौरसेनी अपभ्रंश
- अर्द्ध-मागधी अपभ्रंश
- नागर अपभ्रंश
Ans (2): ब्रज भाषा का आधार भाषा शौरसेनी अपभ्रंश रही है। शौरसेनी अपभ्रंश से तीन उपभाषाओं का विकास हुआ- पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियाँ आती हैं- खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी।
97. अवधी भाषा की शब्दावली-
- तत्सम बहुला है।
- देशज बहुला है।
- तद्भव बहुला है।
- विदेशी शब्द बहुला है।
Ans (3): अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ आती हैं- अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत आती है। यह अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फ़ैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहबाद, जौनपुर आदि जिलों में बोली जाती है।
98. वाक्य-संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा-
- अंग्रेजी भाषा की भाँति अयोगात्मक, अविभक्तिक या स्थान प्रधान है
- संस्कृत भाषा की भाँति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है।
- बंगला भाषा की भाँति अयोगात्मक, अविभक्तिक या स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्तिकता की ओर बढ़ रही है।
- चीनी भाषा की भाँति एक-एक अक्षर में ही पूरे-पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है।
Ans (2): वाक्य-संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भाँति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है।
99. मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, जो-
- कार्य संपादित करनेवालों की सूचना देती है।
- संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है।
- उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है।
- संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है।
Ans (4): मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में करक के 8 भेद हैं।
100. “मैं अपना काम आप करता हूँ।” इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ‘आप’ पद है-
- निकटवर्ती संबंध सूचक सर्वनाम
- निजवाचक सर्वनाम
- गुणवाचक सर्वनाम
- सार्वनामिक विशेषणात्मक सर्वनाम
Ans (2): “मैं अपना काम आप करता हूँ।” इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ‘आप’ पद निजवाचक सर्वनाम है। जब आप शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, परन्तु जब यह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है।
101. अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है, अपनी मूल प्रकृति के-
- आक्षरिक होने का कारण
- अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण
- दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने के दुराग्रह के कारण
- सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण
Ans (1): अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है, अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने का कारण। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ई. में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी।
102. हिंदी भाषा की शब्द-संपदा में सम्मिलित है-
- तत्सम और तद्भव शब्द
- तत्सम और देशज शब्द
- तत्सम, तद्भव, देशज, देशी और विदेशी शब्द
- शहरी और ग्रामीण शब्द
Ans (3): हिंदी भाषा की शब्द-संपदा में तत्सम, तदभव, देशज, देशी और विदेशी शब्द सम्मिलित हैं।
- तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं।
- तदभव संस्कृत के वे शब्द हैं जो भाषा की विकास यात्रा में विकृत होकर हिंदी में पहुँचे हैं।
- देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक श्रोत नहीं होता है। ये बोलचाल में स्वत: निर्मित हो जाते हैं।
- विदेशी वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओँ से हिंदी में आए हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओँ के शब्द हिंदी में बहुतायत में पाए जाते हैं।
103. हिंदी कवियों/रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गार्सा द तासी ने 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में, शिवसिंह सेंगर ने 1883 में और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम में बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि-
- यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है।
- इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि।
- यह कवि-परिचय के साथ कविकर्म का भाषावैज्ञानिक मूल्यांकन करता है।
- हिंदी के कवियों की मुक्त कंठ से सराहना करता है।
Ans (2): कालक्रम में बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि मौजूद है। जॉर्ज ग्रियर्सन का फ्रेंच भाषा में रचित ‘द मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान’ ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है।
104. हिंदी-साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न-भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि-
- हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न-भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो।
- भाषा-सुबोधता की दृष्टि से उसकी सभी विभाषाएँ सुबोध्य हैं।
- हिंदी के सभी समीक्षकों ने उसे एक भाषा के अन्तर्गत ही माना है।
- आज भी उसकी सभी विभाषाओं में एक ही स्तर की श्रेष्ठ रचनाएँ की जा रही हैं।
Ans (1): हिंदी-साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न-भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न-भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो।
105. हिंदी साहित्य के आदिकाल को ‘सिद्ध-सामंत युग’ नाम दिया है-
- हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
- डॉ. रामकुमार वर्मा ने
- रामचंद्र शुक्ल ने
- राहुल सांकृत्यायन
Ans (4): हिंदी साहित्य के आदिकाल को ‘सिद्ध-सामंत युग’ नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है।
आदिकाल का नामकरण-
- जार्ज ग्रियर्सन- चारणकाल
- रामचंद्र शुक्ल- वीरगाथा काल
- मिश्रवंधु- प्रारम्भिक काल
- महावीर प्रसाद द्विवेदी- बीजवपन काल
- राहुल सांकृत्यायन- सिद्ध-सामंत काल
- रामकुमार वर्मा- संधि एवं चारण काल
- हजारी प्रसाद द्विवेदी- आदिकाल
106. हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को ‘श्रृंगारकाल’ नाम दिया है-
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
- नलिन विलोचन शर्मा
- डॉ. गुलाब राय
- डॉ. नगेंद्र
Ans (1): हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को ‘श्रृंगारकाल’ नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है।
उत्तर मध्यकाल का नामकरण-
- जार्ज ग्रियर्सन- रीतिकाव्य
- मिश्रवंधु- अलंकृत काल
- रामचंद्र शुक्ल- रीति काल
- रमाशंकर शुक्ल ‘रसाल’- कला काल
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र- श्रृंगार काल
107. विद्यापति की भक्ति-श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है?
- हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की
- हिंदी साहित्य के मध्य काल की
- हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की
- हिंदी साहित्य के आदिकाल की
Ans (4): विद्यापति की भक्ति-श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव श्रृंगार के कवि हैं।
विद्यापति को बच्चन सिंह ने ‘जातीय कवि’, हर प्रसाद शास्त्रीय ने ‘पंचदेवोपासक’, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि’ कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है- “आध्यात्मिक रंग के चश्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने ‘गीतगोविंद’ को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी।”
108. आल्ह खण्ड का वास्तविक स्त्रोत ग्रंथ है-
- खुमाण रासो
- विजयपाल रासो
- परमाल रासो
- पृथ्वीरज रासो
Ans (3): आल्ह खण्ड का वास्तविक स्त्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। इस ग्रंथ में महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके रचयिता जगनिक हैं। आल्हाखंड को सर्वप्रथम वर्ष 1865 ई. में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश ‘चार्ल्स इलियट’ ने प्रकाशित कराया था। आल्हा बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है।
109. “महुअर बुज्झइ कुसुम रस, कब्ब कलासु छइल्ल।
सज्जन पर उअआर मन, दुज्जन नाम मइल्ल॥”
-ये किस कवि की पंक्तियाँ है?
- सरहपाद की
- कुशललाभ की
- उमापति की
- विद्यापति की
Ans (4): उपरोक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है।
110. आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए, उसे ‘हिन्दवी’ कहा-
- राहुल सांकृत्यायन ने
- अमीर खुसरो ने
- डॉ. श्यामसुंदर दास ने
- क्षितिमोहन सेन ने
Ans (2): आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए, उसे ‘हिन्दवी’ अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें खड़ीबोली का आदि कवि माना जाता है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर ग्यारह राजाओं का आरोहण देखा था।
111. श्रृंगार रस में आकण्ठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि-वर्ग था-
- चारण कवि
- अष्टछापी कवि
- काव्यशास्त्र के आचार्य कवि
- घुमन्तू प्रवृत्ति के लोक कवि
Ans (1): श्रृंगार रस में आकण्ठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि-वर्ग चारण कवि था।
112. इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं-
- स्वयंभू
- धनपाल
- रामसिंह
- कुशललाभ
Ans (1): अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू को जैन परम्परा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को ‘देशीभाषा’ कहा है। पउमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ और स्वयंभू छंद इनके तीन प्रमुख ग्रंथ हैं।
113. निर्गुनियाँ संतों की काव्य-सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है-
- आदिकाल लोक-कथाओं पर
- नाथों की रचनाओं पर
- दक्षिण भारत के वीर शैवों की भक्ति भावना पर
- सूफियों की यौगिक साधना पर
Ans (2): निर्गुनियाँ संतों की काव्य-सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। नाथों से ही कबीर ने हठयोग की अवधारणा ग्रहण की थी।
114. ‘चन्दायन’ के रचयिता हैं-
- मलिक मुहम्मद जायसी
- कुतुबन
- मंझन
- मुल्ला दाऊद
Ans (4): ‘चन्दायन’ के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी काव्य परम्परा का पहला ग्रंथ माना है। चंदायन को माताप्रसाद गुप्त ने ‘लोरकथा’ या ‘लोरकहा’ कहा है। इसकी भाषा अवधी है तथा यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है।
115. निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं-
- दादूदयाल
- हरिदास
- गरीबदास
- सुंदरदास
Ans (2): निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। सिद्वांत के पद और केलिमाल इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं।
116. ‘भक्तमाल’ के रचयिता का नाम है-
- नाभादास
- अग्रदास
- प्राणनाथ
- सुंदरदास
Ans (1): ‘भक्तमाल’ के रचयिता का नाम नाभादास है। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। जार्ज ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम ‘नारायणदास’ बतलाया है। नाभादास ने 1585 ई. के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। इसमें 200 कवियों का जीवनवृत्त 316 छाप्पयों में लिखा गया है। वर्ष 1712 ई. में प्रियदास ने ‘भक्तमाल की टीका ‘रसबोधिनी’ शीर्षक से ब्रजभाषा के कविन्त सवैया शैली में लिखी।
117. “भक्तन को कहा सीकरी सों काम” यह किस कवि की उक्ति है?
- नंददास
- परमानंद दास
- कुंभनदास
- तुलसीदास
Ans (3): यह उक्ति कुंभनदास की है। कुंभनदास पुष्टिमार्ग के संथापक बल्लभाचार्य के शिष्य एवं अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कवि थे। अकबर के फतेहपुर सीकरी निमंत्रण पर इन्हें काफी ग्लानि हुई थी तब इन्होंने यह उक्ति कही थी।
118. “हिंदी नयी चाल में ढली” यह कथन है-
- महावीर प्रसाद द्विवेदी का
- डॉ. श्यामसुंदर दास का
- राधाकृष्ण दास का
- भारतेंदु हरिश्चंद्र का
Ans (4): “हिंदी नयी चाल में ढली” सन् 1873 ई.- यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चन्द्री हिंदी’ कहा है। साथ ही उन्हें सिद्ध वाणी का सरल सहृदय कवि भी कहा है।
119. ‘द्विवेदी-युग’ का नामकरण किया गया है-
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर
- शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर
- महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर
- सोहनलाल द्विवदी के नाम पर
Ans (3): ‘द्विवेदी-युग’ का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। हिंदी साहित्येतिहास में 1900 ई. से लेकर 1920 ई. तक के काल को द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को रामचंद्र शुक्ल ने ‘बातों का संग्रह’ कहा है।
120. छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी-
- मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में
- सुमित्रानंदन पंत की कविता में
- सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ में
- श्रीधर पाठक में
Ans (1): छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में दिखाई पड़ी। मुकुटधर पांडेय ने छायावाद शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में वर्ष 1920 ई. में ‘हिंदी में छायावाद’ शीर्षक से चार किस्तों में लेख प्रकाशित करवाया था।