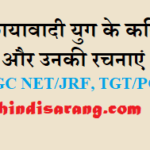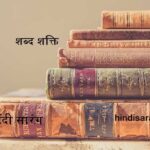सर्वनाम की परिभाषा
संज्ञा के बार-बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम (pronoun) कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे सर्वनाम (sarvnam) कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में- “सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, जो पूर्वापरसंबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है।”1 संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है, जिसका वह (संज्ञा) नाम है, जैसे गाय कहने से केवल गाय का बोध होता है, बैल, भैंस, बकरी, पेड़ आदि का नहीं। परंतु ‘वह’, ‘यह’ आदि कहने पर पूर्वापरसंबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे-
- रमेश ने कहा की मैं बीमार हूँ। (‘रमेश’ के स्थान पर ‘मैं’)
- सभी लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं। (‘लोगों’ के स्थान पर ‘हम’)
- राधा ने कृष्ण से पूछा कि तुम कब जाओगे। (‘कृष्ण’ के स्थान पर ‘तुम’)
- रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है। (‘रोटी’ के स्थान पर ‘वह’)
उपरोक्त वाक्यों में मैं, हम, तुम, वह सर्वनाम हैं।
सर्वनाम किसे कहते हैं?

वाक्य में एक बार प्रयुक्त संज्ञापद के स्थान पर उसे सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं; जैसे- मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह आदि।
सर्वनाम के भेद:

हिंदी में कुल ग्यारह सर्वनाम हैं- मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के छह भेद होते हैं-
- पुरुषवाचक सर्वनाम
- निश्चयवाचक सर्वनाम
- अनिश्चयवाचक सर्वनाम
- प्रश्नवाचक सर्वनाम
- संबंधवाचक सर्वनाम
- निजवाचक सर्वनाम
1. पुरुषवाचक सर्वनाम (personal pronoun)

“पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों (स्त्री या पुरुष) के नाम के बदले आते हैं।”2 जो सर्वनाम बोलनेवाले, सुननेवाले और किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे- मैं, तू और वह पढ़ेंगे।
उपर्युक्त वाक्य में वार्तालाप के समय तीन पुरुष हैं। कहने वाला पुरुष- मैं, सुननेवाला पुरुष- तू और जो पुरुष बातचीत में उपस्थित नहीं- वह। लेखक या वक्ता को उत्तमपुरुष, पाठक या श्रोता को मध्यपुरुष और शेष सब अन्य पुरुष में होते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हुए।
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद:
पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं-
- (a) उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम
- (b) मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
- (c) अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
(a) उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम:
बोलनेवाले या लिखनेवाले के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- मैं, हम, मुझको, मैंने, मुझे आदि। यद्यपि ‘हम’ शब्द बहुवचन है लेकिन इसका प्रयोग एकवचन के रूप में भी किया जाता है।
उदाहरण-
- मैं घर जाऊँगा।
- हम भगवान को नहीं देख सकते।
- यह निबंध मैंने लिखा है।
- मुझे सिनेमा देखना नहीं पसंद।
(b) मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम:
बात सुननेवाले (श्रोता) के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, तेरा आदि।
उदाहरण-
- तू कुछ भी बोल देता है।
- तुम अब बोल सकती हो।
- तुम्हें कुछ कहना बेकार है।
- आप मेरे गुरु हैं।
- तुम्हारा घर बहुत दूर है।
- तेरा बैग बहुत भारी है।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधी अन्य तथ्य-
- प्रायः बातचीत में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों का बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे- तुम यहाँ अकेले मत ठहरो।
- ‘तू’ शब्द का एक वचन में प्रयोग या तो अपने से बहुत छोटों के लिए किया जाता है या किसी का निरादर करने के लिए। जैसे-
- मैं तुझे अभी बाहर का रास्ता दिखाता हूँ।
- बेटा! तू यहीं रुक। मैं तेरे लिए बिस्किट लेते आऊंगा।
- ‘तू’ शब्द का प्रयोग बहुत अधिक घनिष्ठता, अपनापन या श्रद्धा जताने के लिए भी किया जाता है। जैसे-
- तू तो मेरे भाई जैसा है, तब तू इतना क्यों लजा रहा।
- हे भगवान्! तू ही हमारा रक्षक है।
- ‘आप’ शब्द का प्रयोग किसी को आदर या सम्मान देने के लिए किया जाता है। जैसे-
- आप हमारे लिए भगवान हैं।
- आप हमारे पूज्य हैं।
(c) अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम:
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर अन्य सब संज्ञाओं के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- यह, वह, वे, ये, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि।
उदाहरण-
- वह कल खेलने नहीं आया था।
- वे नहीं आयेंगे।
- उन्होंने वादा किया है।
- उसे कल बुला लेना।
- उन्हें जाने दो।
- इनसे कहिए कि मुझे परेशान न किया करें।
इसे भी देखें-
2. निश्चयवाचक सर्वनाम (demonstrative pronoun)

“जो सर्वनाम पास की या दूर की किसी खास वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।”3 दूसरे शब्दों में- सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चत रूप से बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- यह, वह आदि।
उदाहरण-
- यह कोई नया काम नहीं है।
- रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है।
निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद:
निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार का होता है- दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम।
(a) दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम:
जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं उन्हें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ‘वह’ दूर के पदार्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे- वह मेरी पैन है। वे किताब हैं।
इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं।
(b) निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम:
जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराये उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ‘यह’ निकट के पदार्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे- यह मेरी पैन है। ये मुझे बहुत पसंद है।
इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही है।
निश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी अन्य तथ्य:
- दो संज्ञाओं में से पहली के लिए ‘यह’ और दूसरी के लिए ‘वह’ का प्रयोग किया जाता है। जैसे- कोयल और कौए में यही भेद है कि यह मधुर बोलता है और वह कुवचन।
- ‘यह’ शब्द कभी-कभी वाक्य या वाक्यांश की ओर भी संकेत करता है। जैसे- जन-मन-गन—यह हमारा राष्ट्रीय गीत है।
- ‘वह’ का पुराना रूप ‘सो’ है, इसका प्रयोग आज भी कभी-कभी होता है।
3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (indefinite pronoun)

“जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।”4 अर्थात जो सर्वनाम ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराये जिसका निश्चय न हो पाये। जैसे- कोई, कुछ आदि। सब कोई, हर कोई, कोई और, सब कुछ, कुछ का कुछ आदि भी अनिश्चयवाचक प्रयोग हैं।
उदाहरण-
- कोई आया था
- ऐसा न हो कि कोई आ जाए।
- बैग में कुछ नहीं है।
- उसने कुछ नहीं खाया।
- कई ईश्वर तक को नहीं मानते।
- हर कोई जल्दबाजी में ही रहता है।
4. प्रश्नवाचक सर्वनाम (interrogative pronoun)

“जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।”5 दूसरे शब्दों में- जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, उन्हें प्रश्रवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- कौन, क्या आदि।
उदाहरण-
- कौन है दरवाजे पर?
- कौन आया था?
- तुम क्या खा रहे हो?
- क्या चाहते हो?
- तुम क्या लाये हो?
‘कौन’ और ‘क्या’ में विशेष अंतर यह है कि ‘कौन’ का प्रयोग प्राय: प्राणियों या चेतन जीवों के लिए और ‘क्या’ का प्रयोग जड़ पदार्थों या भाववाचक संज्ञाओं के लिए होता है। जब ‘क्या’ का अर्थ आश्चर्य या अन्यवचन आदि के लिए हो तब यह सर्वनाम न रहकर क्रियाविशेषण बन जाता है। जैसे-
- क्या कहने तुम्हारे!
- मैं उसे समझाता ही क्या हूँ?
- क्या गोरे क्या काले सबको एक दिन मरना है। (यहाँ ‘क्या’ समुच्चयबोधक है।)
- स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत क्या से क्या हो गया! (यहाँ ‘क्या’ वाक्यांश के रूप में आया है।)
5. संबंधवाचक सर्वनाम (relative pronoun)

जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वशुदेवनंदन प्रसाद के शब्दों में, “ जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।”6 जैसे- जो, सो आदि।
उदाहरण-
- जो जागत है सो पावत है।
- वह जो न करे, सो थोड़ा।
- वह कौन है, जो पड़ा रो रहा।
कभी-कभी संबंधवाचक सर्वनाम की कल्पना करनी पड़ती है, उसका प्रयोग हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे-
- गया सो गया।
- हुआ सो हुआ।
उपरोक्त वाक्यों में ‘जो’ शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है।
6. निजवाचक सर्वनाम (reflexive pronoun)

‘निज’ का अर्थ होता है- अपना और ‘वाचक’ का अर्थ होता है- बोध (ज्ञान) कराने वाला अर्थात ‘निजवाचक’ का अर्थ हुआ- अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार, ‘स्वंय’ अर्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- आप।
उदाहरण-
- हम आप कर लेंगे।
- तुम आप देख लोगे।
- मैं आप ही चलता हूँ कि सबसे अलग रहूँ।
- यह आप ही आप बकता जा रहा है, इसे किस ने बुलाया।
उपरोक्त वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की चर्चा करने के लिए उसी वाक्य में ‘आप’ सर्वनाम आया है। पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक वाले ‘आप’ से इसका प्रयोग भिन्न है। यह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। वहीं पुरुषवाचक ‘आप’ बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे-
- आप मेरे सिर-आखों पर है। (आदरसूचक)
- मैं आप ही आ जाऊँगा। (निजवाचक)
निजवाचक ‘आप’ एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
निजवाचक सर्वनाम ‘आप’ का प्रयोग निम्नलिखित अर्थो में होता है-
- निजवाचक ‘आप’ का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण (निश्चय) के लिए होता है। जैसे- मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ।
- निजवाचक ‘आप’ का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे- उन्होंने मुझे रहने को कहा और ‘आप’ चलते बने, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है।
- सर्वसाधारण के अर्थ में भी ‘आप’ का प्रयोग होता है। जैसे- आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है।
- अवधारण के अर्थ में कभी-कभी ‘आप’ के साथ ‘ही’ जोड़ा जाता है। जैसे- मैं आप ही चला आता था, वह काम आप ही हो गया। मैं वह काम ‘आप ही’ कर लूँगा।
- ‘आप’ के स्थान पर कभी-कभी ‘स्वंय’, ‘खुद’, ‘स्वत:’ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे- गांधीजी स्वंय सत्यवादी थे और दूसरों को भी सत्य का उपदेश देते थे।, जो खुद नहीं करता उसे दूसरों को कहने का क्या अधिकार है?
संयुक्त सर्वनाम:
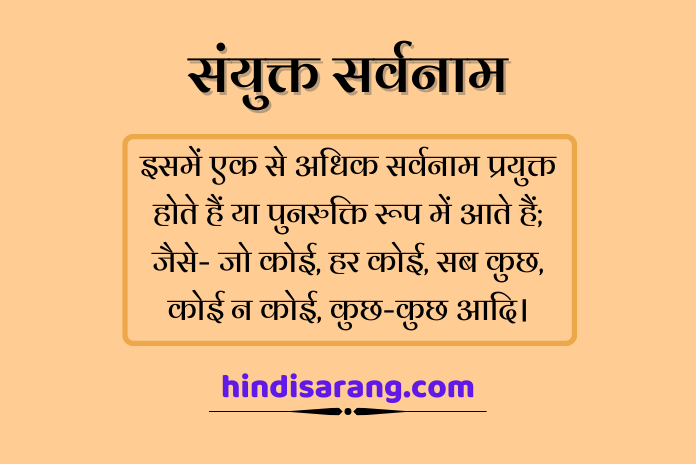
कभी-कभी दो या दो से अधिक सर्वनाम इकट्ठे प्रयुक्त होते हैं, अथवा एक सर्वनाम पुनरुक्त रूप में आ जाते हैं। इसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। रूस के हिंदी वैयाकरण डॉ. दीमशित्स ने इसकी खोज और नामकरण किया था। उन्हीं के शब्दों में, “संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है, क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा-शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है।”7 जैसे- जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, कुछ और, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई-न-कोई, कुछ-न-कुछ, कुछ-कुछ, कोई-कोई इत्यादि।
सर्वनाम के रूपांतरण:
सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंगभेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। जैसे-
- वह खाता है।
- वह खाती है।
इसलिए सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही रूप होता है। केवल संबंधकारक में कुछ एक सर्वनामों से लिंगभेद प्रगट होता है। जैसे- मेरा-मेरी, तेरा-तेरी, हमारा-हमारी, तुम्हारा-तुम्हारी।
संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं- एकवचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्तिरहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं।
सर्वनाम में केवल सात कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। कारकों की विभक्तियाँ लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है। जैसे-
- मैं- मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा
- तुम- तुम्हें, तुम्हारा
- हम- हमें, हमारा
- वह- उसने, उसको उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको
- यह- इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे
- कौन- किसने, किसको, किसे
Sarvanam MCQ’s:
निजवाचक सर्वनाम
- आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद, पृष्ठ-115 ↩︎
- वही ↩︎
- सुगम हिंदी व्याकरण- वंशीधर, पृष्ठ- 63 ↩︎
- आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद, पृष्ठ-116 ↩︎
- व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना- हरदेव बाहरी, पृष्ठ- 86 ↩︎
- आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद, पृष्ठ-116 ↩︎
- [7] वही, पृष्ठ-117 ↩︎