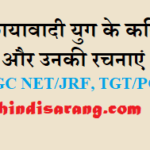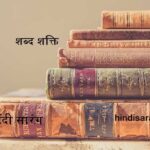रीतिबद्ध कवि
जिन कवियों नें शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना किया उन्हें रीतिबद्ध श्रेणी में रखा गया है। हिन्दी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्न हैं-
| रचनाकार | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|
| चिन्तामणि | मुक्तक काव्य: रस विलास, छन्द विचार, पिगल, श्रृंगार मंजरी,कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार प्रबंध काव्य: रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्णचरित |
| कुलपति मिश्र | रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नख शिख, द्रोण पर्व |
| कुमार मणि | रसिक रंजन, रसिक रसाल |
| देव | भावविलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देवमाया प्रपंच (नाटक), रस विलास, रस रत्नाकर, सुख सागर तरंग |
| सोमनाथ | रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद |
| भिखारीदास | रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंजशतिका |
| रसिक गोविन्द | रसिक गोविन्दानन्दघन, पिंगल, रसिक गोविन्द, युगल रस माधुरी, समय प्रवन्ध, लछिमन चंद्रिका, अष्टदेश भाषा |
| प्रताप साहि | व्यंग्यार्थ कौमुदी (1825 ई.), काव्य विलास (1809 ई.), जयसिह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, शृंगार शिरोमणि, अलंकार चिन्तामणि, काव्य विनोद, जुगल नखशिख |
| अमीरदास | सभा मंडन (1827 ई.), वृत्त चन्द्रोदय (1820 ई.), व्रजविलास सतसई (1832 ई.), श्री कृष्ण साहित्य सिन्धु (1833 ई.), शेर सिंह प्रकाश (1240 ई.), फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रलाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व-संहिता प्रकाश |
| ग्वाल | यमुना लहरी, भक्त भावन, रसरूप, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, विजय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, वंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षड्ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, दृग शतक, हम्मीर हठ |
| तोष निधि | सुधा निधि, नख शिख, विनय शतक |
| रसलीन | रस प्रबोध (1741 ई.), अंग दर्पण (1737 ई.) |
| पद्माकर भट्ट | हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगालहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कलि पच्चीसी |
| वेनी ‘प्रवीन’ | श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग (1817), नानाराव प्रकाश। |
| सुखदेव मिश्र | वृत्तविचार, छंदविचार, फाजिल अलीप्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता |
| याकूब खाँ | रस भूषण (1812 ई.) |
| उजियारे (दौलत राम) | रसचंद्रिका, जुगलरस प्रकाश |
| राम सिंह | जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास |
| चंद्रशेखर वाजपेयी | रसिक विनोद, नख शिख, वृन्दावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हम्मीर हठ (प्रबन्ध काव्य) |
| मतिराम | फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंदसार संग्रह (वृत्ति कौमुदी) |
| कृष्ण भट्ट देव ऋषि | श्रृंगार रसमाधुरी (1712 ई.), अलंकार कलानिधि |
| कालिदास त्रिवेदी | वारवधूविनोद, राधामाधव बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा |
| जसवंत सिंह | भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव प्रकाश, आनन्द विलास, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त सार |
| भूषण | शिवराज भूषण (1673), शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा |
| गोप | रामालंकार, रामचंद्रभूषण, रमाचंद्रभरण |
| रसिक सुमित | अलंकार-चन्द्रोदय (1729 ई.) |
| रघुनंदन वन्दीजन | रसिक मोहन (1739 ई.), काव्य कलाधर (1745 ई.), जगत मोहन (1750 ई.) |
| दूलह | कविकुलकंठाभरण |
| रस रूप | तुलसीभूषण (1754 ई.) |
| सेवादास | नखशिख, रसदर्पण, गीता माहात्म्य, अलबेले लाल जू को नख शिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार |
| मंडन | रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्यरत्न, नैन पचासा, जनक पच्चीसी |
| गिरिधरदास | भारती भूषण (1833 ई.) |
| भूषण ‘मुरलीधर’ | छन्दो हदय प्रकाश (1666 ई.), अलंकार प्रकाश (1648 ई.) |
| राम सहाय | वृत्त तरंगिणी (1816 ई.), अलंकार प्रकाश (1648 ई.), वाणी भूषण |
| माखन | श्रीनाग पिंगल अथवा छंदविलास (1702 ई.) |
| दशरथ | वृत्त विचार (1799 ई.) |
| सूरति मिश्र | अलंकार माला, रसरत्न माला, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धान्त, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर |
| उदयनाथ कवीन्द्र | रसचन्द्रोदय, विनोद चन्द्रिका, जोगलीला |
प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त निम्नांकित है-
| कवि | जन्म-मृत्यु | जन्म स्थान | आश्रयदाता |
|---|---|---|---|
| चिन्तामणि त्रिपाठी | 1809-1685 | तिकवाँपुर | 1. शाहजी भोंसला, 2. शाहजहाँ, 3. दाराशिकोह |
| भूषण | 1613-1715 | तिकवापुर | 1. शिवा जी, 2. छत्रसाल |
| मतिराम | 1617 | तिकवांपुर | 1. जहाँगीर, 2. कुमायूँ नरेश ज्ञानचंद, 3. राव भाव सिंह हाड़ा, 4. स्वरूप सिंह बुन्देला |
| जसवंत सिंह | 1626-1688 | मारवाड | ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे |
| सुखदेव मिश्र | – | रायबरेली | – |
| तोष निधि | – | श्रृंगवेरपुर | 1. भगवंत राय खाची 2. राव मर्दन सिंह 3. देवी सिंह 4. फाजिल अली शाह |
| कुलपति मिश्र | – | आगरा | रामसिंह |
| देव (देवदत्त) | 1673-1767 | इटावा | 1. आजमशाह, 2. भवानीदत्त वैश्य, 3. कुशल सिंह, 4. सेठ भोगीलाल (मोतीलाल), 5. उद्योत सिह, 6. सुजान मणि, 7. अली अकबर खाँ |
| सैयद गुलामनबी | 1699-1750 | बिलग्राम | |
| रसलीन | – | हरदोई | |
| भिखारीदास | – | ट्योंगा, प्रतापगढ़ | हिन्दूपति सिंह |
| पद्माकर | 1753-1833 | बाँदा | 1. रघुराव अप्पा, 2. महाराज जैतपुर, 3. नोने अर्जुन सिंह 4. पारीक्षित, 5. अनूपगिरि (हिम्मत बहादुर), 6. रघुनाथ राव, 7. प्रताप सिंह, 8. जगत सिंह, 9. भीम सिंह, 10. दौलत राव सिंधिया |
केशवदास
केशवदास का जन्म 1560 ई. और मृत्यु 1617 ई. में हुई थी। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा रामसिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा में रहते थे। केशव सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर काव्य-रीति के विभिन्न अंगों का सम्यक विवेचन करने वाले आचार्य हैं। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ परम्परा के प्रवर्तक केशवदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी और उनके परवर्ती कवियों को रसवादी माना है। केशवदास अलंकार को कविता के लिए महत्त्वपूर्ण मानते थे, उन्होंने लिखा भी है-
“जदपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्ति
भूषण बिंदु न विराजई कविता बनिता मित्त।।”
रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा है, लेकिन प्रवृति की दृष्टि वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है क्योंकि उनकी कविता में अलंकार, चमत्कार एवं पांडित्य प्रदर्शन का भाव प्रमुख है।
केशवदास के ग्रन्थों का विवरण निम्नलिखित है-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विषय वस्तु |
| मुक्तक | ||
| रसिकप्रिया | 1591 | लक्षण ग्रंथ, नवरसों का निरूपण |
| कविप्रिया | 1601 | अलंकारों का निरूपण |
| छंदमाला | 77 छंदों का निरूपण | |
| नखशिख | – | – |
| महाकाव्य | – | – |
| रामचंद्रिका | 1601 | – |
| रतनबावनी | 1607 | – |
| वीरसिंह देव चरित | 1607 | – |
| विज्ञानगीता | 1607 | आध्यात्मिक विषयों को प्रतीक शैली में प्रस्तुत किया गया है |
| जहांगीरजसचन्द्रिका | 1612 | – |
1. रामचंद्रिका
जनश्रुति के अनुसार केशव ने रामचंद्रिका की रचना बाल्मीकि के द्वारा स्वप्न में कहने पर किया था। रामचंद्रिका में ‘छंदों का वैविध्य’ या छंदों की भरमार’ मिलता है। इन्होंने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में किया था। परंतु रामचंद्रिका का मूलाधार बाल्मीकि रामायण है। केशवदास की रामचंद्रिका महाकाव्य प्रसन्नराघव, हनुमन्नाटक, अनर्धराघव, कादम्बरी और नैषध ग्रंथों से प्रभावित है। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है की “केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला।
2. रसिकप्रिया
केशवदास ने रसिकप्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रबीन को शिक्षा देने के लिए की थी। यह ग्रंथ 16 प्रकाशों में विभक्त है जिसमें 13 प्रकाशों में श्रृंगार विवेचन और शेष 3 में अन्य रसों, वृतियों तथा काव्य दोषों का विवेचन मिलता है।
3. कविप्रिया
इस ग्रंथ में केशवदास ने अलंकारों के निरूपण के साथ काव्य रीति, दोष आदि का भी विवेचन किया है।
केशवदास के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के कथन-
1. केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए।
2. कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था।
3. केशव केवल उक्तिवैचित्र्य और शब्दक्रीडा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी।
4. इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक समावेश पहले-पहल आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परम्परा का प्रवाह केशव की ‘कविप्रिया’ के प्राय: पचास वर्ष पिछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं।
5. प्रबंध रचना योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति
नोट: आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य माना है-
1. संबंध निर्वाह
2. कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान
3. दृश्यों की स्थानगत् विशेषता
केशवदास की रचनाओं के टीकाकार
| रचनाएँ | टीका | टीकाकार | भाषा |
|---|---|---|---|
| रसिकप्रिया | रसग्राहकचंद्रिका | सुरति मिश्र | ब्रज |
| रसिकप्रिया | तिलक | हरिचरणदास | ब्रज |
| कविप्रिया | जोरावरप्रकाश | सुरति मिश्र | ब्रज |
| कविप्रिया | कविप्रिया भरण-तिलक | हरिचरणदास | ब्रज |
चिन्तामणि त्रिपाठी
चिंतामणि का जन्म 1609 ई. में कानपुर में हुआ था। रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि त्रिपाठी को रीतिकाव्य का प्रवर्तक माना है। चिन्तामणि त्रिपाठी सिद्धान्ततः रसवादी थे। इनके के भाई मतिराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमाला भी लिखा है। चिन्तामणि त्रिपाठी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है।
चिन्तामणि की रचनाएँ:
1. मुक्तक काव्य:
रस विलास, छन्द विचार, पिगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार
2. प्रबंध काव्य:
रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्णचरित
कविकुल कल्पतरु में काव्य के दशांगों का विवेचन हुआ है। इसमें इसमें 1133 पद्य हैं और यह 8 प्रकरणों में विभक्त है। ‘रसविलास’ रस विवेचन का ग्रंथ है। वहीं ‘श्रृंगार मंजरी’ नायक-नायिका भेद [आंध्रप्रदेश कर संत अकबरशाह के श्रृंगार मंजरी (संस्कृत) का ब्रजभाषा में अनुवाद] इसी तरह ‘छंद विचार’ पिंगल प्राकृत पैंगल तथा भट्टकेदार के ‘वर्णरत्नाकर’ को आधार बनाकर कृष्ण का चरित-वर्णन किया गया है।
भिखारीदास
भिखारीदास का जन्म 1750 ई. के आस-पास टोंग्या में हुआ था। इनके आश्रयदाता हिन्दूपति (प्रतापगढ़ नरेश पृथ्वीसिंह के अनुज) थे। इनकी प्रमुक रचनाएँ निम्नलिखित हैं-
| रचनाएँ | विशेषता |
|---|---|
| रस सारांश | काव्यांग विवेचन |
| काव्य निर्णय | काव्यांग विवेचन |
| श्रृंगार निर्णय | काव्यांग विवेचन, श्रृगार विषयक |
| छंदोवर्ण पिंगल | काव्यांग विवेचन |
| छंद प्रकाश | – |
| नाम प्रकाश | – |
| विष्णुपुराण भाषा | – |
| शतरंजशतिका | शंतरंज के खेल संबंधी |
| शब्दनाम कोश | – |
| अमरकोश | – |
भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिन्दी काव्य-परम्परा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माना जाता है। ‘काव्य निर्णय’ इनका प्रमुख ग्रंथ है जो 25 उल्लासों में विभक्त है। इसकी रचना हिंदूपति सिंह के नाम पर की गई है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि, ‘दास जी ऊँचे दर्जे के कवि थे।’ मिश्रबंधुओं ने ‘मिश्रबंधुविनोद’ में अलंकृतकाल (रीतिकाल) को दो भागों में विभाजित किया-
- पूर्वालंकृतकाल: का सबसे बड़ा आचार्य चिंतामणि को माना है।
2. उत्तरालंकृतकाल: का सबसे बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना है।
भूषण
भूषण का जन्म 1631 ई. में तिकवांपुर में हुआ था और मृत्यु 1715 ई. में हुआ था। भूषण की समग्र रचनाएँ मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। इनके ग्रन्थों का विवरण निम्नलिखित है-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विशेषता | आश्रयदाता |
| शिवराज भूषण | 1673 | अलंकार ग्रंथ, 105 अलंकारों का निरूपण, 284 छंदों में वर्णित | छत्रपति शिवाजी |
| शिवा बावनी | शिवा जी की वीरता का वर्णन | छत्रपति शिवाजी | |
| छत्रसाल दशक | छत्रसाल की वीरता का वर्णन | – |
भूषण के उपरोक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं परंतु कुछ विद्वान् 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं- भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा।
भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे। भूषण ने इन्हीं दो नायकों को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि, ‘प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दीनों प्रधान्य था, उसमें वीर रस की रचना की यही उनकी विशेषता है।’ आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि, “इन दी वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।” भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाह ने इन्हें ‘कवि भूषण’ उपाधि दी थी। रीतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की तरफ मोड़ने का श्रेय भूषण को ही है। गणपतिचन्द्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम ‘पतिराम’ या ‘मनीराम’ बताया है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूलनाम ‘घनश्याम’ बताया है।
महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कन्धा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था – “सिवा को बखान कि बखानौ छत्रसाल को।” भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष भाषागत् अव्यवस्था (शब्दों को तोड़-मरोड़ कर विकृत करना) और व्याकरणगत त्रुटियाँ हैं। ‘शिवराज भूषण’ में इन्होंने दोहे में अलंकारों की परिभाषा दिया है और कवित्त एवं सवैया छंद में उदाहरण दिये हैं। इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। शिवराज भूषण में लक्षण और उदाहरण जयदेव के ‘चंद्रलोक’ तथा मतिराम के ‘ललित ललाम’ के आधार पर दिए गये हैं।
रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-
1. भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हदय की सम्पति हुए।
2. शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता।
3. वे हिन्दू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।
मतिराम
मतिराम का जन्म 1604 ई. और मृत्यु 1701 ई. में हुआ था। ये चिंतामणि और भूषण के भाई थे। इनके ग्रन्थों का विवरण निम्नलिखित है-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विषय वस्तु | आश्रयदाता |
| फूलमंजरी | 1619 | 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन | जहांगीर |
| रसराज | 1663 | श्रृंगार रस निरूपण, नायक-नायिका भेद | स्वतंत्र रूप से |
| ललितललाम | 1664 | अलंकार निरूपण | भावसिंह हाडा |
| सतसई | 1681 | बिहारी सतसई का अनुकरण | भोगनाथ |
| अलंकार पंचशिका | 1690 | अलंकार निरूपण | ज्ञानचंद |
| वृत्तिकौमुदी/ छंदसार | 1701 | छंदों का निरूपण | स्वरूप सिंह बुंदेला |
| लक्षण श्रृंगार | – | – | – |
| साहित्य सार | – | नायिका भेद निरूपण | – |
| मतिराम सतसई | – | – | भोगनाथ |
मतिराम का प्रथम ग्रंथ ‘फूलमंजरी’ है। किन्तु डॉ. बच्चन सिंह ने ‘रसराज’ को ही प्रथम ग्रंथ माना है। इन्होंने ‘फूलमंजरी’ की रचना जहाँगीर की आज्ञा पर आगरा में लिखा था। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है जिसके श्लेषार्थ से नायिका का संकेत मिलता है।
रसराज में श्रृंगार एवं नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की ‘रसमंजरी’ और रहीम के ‘बरवै नायिका भेद’ के आधार पर किया गया है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ ‘रसराज’ और ‘ललितललाम’ हैं। जिसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा की- “रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है।” शुक्ल ने ‘वृत्त कौमुदी’ या ‘छंद सार’ को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है जबकि यह ग्रंथ स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा गया है। शुक्ल के अनुसार, “रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य विद्यमान है।”
मतिराम पर लिखे गये प्रमुख ग्रंथ
मतिराम का सर्वप्रथम विस्तृत जीवन परिचय देने वाला ग्रंथ ‘हिंदी नवरत्न’ है, जिसका मुख्य आधार ‘शिवसिंह सरोज’ है।
| ग्रंथ | लेखक |
| हिंदी नवरत्न | मिश्रबंधु |
| मतिराम ग्रन्थावली | कृष्ण बिहारी मिश्र |
| मतिराम: कवि और आचार्य | महेंद्र कुमार |
| महाकाव्य मतिराम | त्रिभुवन सिंह |
जसवंत सिंह
जसवंत सिंह हिन्दी साहित्य के प्रधान या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रन्थों का विवरण निम्नलिखित है-
| ग्रंथ | विषय वस्तु |
| भाषा भूषण | 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण |
| प्रबोध चंद्रोदय | संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद |
| अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव प्रकाश, आनन्द विलास, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त सार | इन ग्रंथों में वेदान्त विषय का निरूपण हुआ है। |
सुखदेव मिश्र
सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाएँ निम्नांकित हैं-
1. वृत्त विचार (1671 ई.), 2. छंद विचार, 3. फाजिल अली प्रकाश, 4. यार्णव, 5. श्रृंगार लता, 6. अध्यात्म प्रकाश (1698 ई.), 7. दशरथ राय
सुखदेव मिश्र के सन्दर्भ में शुक्ल ने लिखा है, “छंदशास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है।” सुखदेव मिश्र को राजा राजसिंह गौड़ ने ‘कविराज’ की उपाधि दी थी।
तोष
तोष रसवादी है। इनका मूलनाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं-
1. सुधानिधि (1634 ई.), 2. नखशिख, 3. विनयशतक
कुलपति मिश्र
कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनके आश्रयदाता जयपुर के राजा रामसिंह थे। कलपति मिश्र रस ध्वनिवादी थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ई. से 1686 ई. तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विषयवस्तु |
| रस रहस्य | 1670 | मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद |
| द्रोण पर्व | 1680 | महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद |
| युक्तितरंगिणी (अप्राप्य) | 1686 | – |
| नखशिख (अप्राप्य) | – | – |
| संग्राम सार | – | – |
| दुर्गा भक्ति चन्द्रिका | – | नगेन्द्र के अनुसार |
देव
देव का मूल नाम देवदत्त था। ये इटावा (उ. प्र.) के रहने वाले थे। इनका जन्म 1673 ई. और मृत्यु 1767 ई. में हुआ था। देव हित हरिवंश के अनन्य सम्प्रदाय में दीक्षित थे। देव जीवकोपार्जन के लिए अनेक राजाओं और नवाबों के यहाँ भटकते रहे पर कहीं जम न सके। देव सर्वप्रथम औरंगजेब के बेटे आजमशाह के आश्रय में रहे। रीतिकाल के कवियों में एकमात्र कवि देव हैं जो निर्गुण भक्तों की तरह जाति-पांति और ऊँच-नीच का विरोध उसी अक्खड़ता के साथ किया है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। देव के रीति-विवेचन का प्रमुख दोष- रीति निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्य है।
देव के 72 ग्रंथ बताये जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी इनके 23 ग्रंथों का जिक्र हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है परंतु वर्तमान में 15 ही उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम शिवसिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बतायी है। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रन्थों का उल्लेख किया है।
देव की प्रमुख रचनाएँ निम्नांकित हैं-
| ग्रंथ | विषय वस्तु / आधार |
|---|---|
| भाव विलास (1689 ई.) | रस एवं नायक-नायिका भेद का वर्णन हुआ है। |
| अष्टयाम | आठ पहरों के बीच होने वाले नायक-नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। देव ने इस ग्रंथ को अजयशाहू को सुनाया था |
| कुशल विलास | कुशल सिंह के नाम पर आधारित है |
| भवानी विलास | भवानीदत्त वैश्य को समर्पित है |
| जाति विलास | अपनी यात्रा का अनुभव, विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है |
| रस विलास | राजा भोगीलाल को समर्पित रचना है, उन्हीं के आश्रय में लिखा गया है |
| राग रत्नाकर | राग-रागिनियों के स्वरूप का वर्णन (संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ) |
| देवचरित | कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य |
| देवमाया प्रपंच | संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद (कृष्ण के जीवन से संबंधित नाटक) |
| देवशतक | अध्यात्म सम्बन्धी ग्रंथ है जिसमें जीवन-जगत संबंधी असारता का चित्रण हुआ है |
| प्रेमचंद्रिका | राजा उद्योत सिंह को समर्पित |
| शब्द (काव्य) रसायन | लक्षण तथा सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है, शब्द शक्ति, रसादि का वर्णन हुआ है |
| सुखसागर तरंग | देव के अनेक ग्रन्थों से लिए हुए कवित्त-सवैया का संग्रह। अली अकबर खां के आश्रय में लिखा गया |
| सुजान विनोद | सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया |
| प्रेम तरंग | इसमें प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया गया है |
रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियाँ भी बतायी हैं जो निम्न हैं-
1. वृक्ष विलास, 2. पावस विलास, 3. ब्रह्मदर्शन पचीसी, 4. तत्त्व दर्शन पचीसी, 5. आत्मदर्शन पचीसी, 6. जगदर्शन पचीसी, 7. रसानंद लहरी 8. प्रेम दीपिका, 9. नखशिख, 10. प्रेम दर्शन
इनका प्रथम ग्रंथ ‘भावविलास’ है। ‘सुख सागर तरंग’ का सम्पादन मिश्र बन्धुओं के पिता ‘बालदत्त मिश्र’ ने सन् 1897 ई. में किया। नगेन्द्र ने ‘सुखसागर तरंग’ को नायिका भेद का ‘विश्वकोश’ माना है। देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ ‘सुखसागर तरंग’ है। ‘शब्द (काव्य) रसायन’ देव का सर्वांगनिरूपक ग्रंथ है, जो 11 प्रकाशों में विभक्त है।रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ‘मध्यकालीन हिन्दी काव्यभाषा’ पुस्तक में लिखा है- देव की ध्वनि-संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्यभाषा में अप्रतिम है।’ विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार ‘देव में उत्कृष्ट बिम्बविधान पाया जाता है।’ रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि, “रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा सम्पन्न कवि थे।”
रसलीन
रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विषय निरूपण |
| अंग दर्पण | 1737 | 1741 दोहों का संग्रह (शुक्ल के अनुसार 1154)नायक-नायिका भेद, अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन |
| रस प्रबोध | 1741 | 1155 दोहे में रसों का वर्णन |
भिखारीदास
भिखारीदास का रचनाकाल 1728-1750 ई. तक माना जाता है। भिखारीदास रीतिकाल के पहले आचार्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम काव्य परम्परा, भाषा, छंद और तुक आदि पर विचार किया। भिखारीदास रीतिकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएँ निम्न हैं-
| ग्रंथ | वर्ष (ई.) | विषय निरूपण |
|---|---|---|
| नाम कोश | 1738 | कोश ग्रंथ |
| रस सारांश | 1742 | रस के भेदोपभेदों का वर्णन |
| छंदार्णव पिंगल | 1742 | छंदों का विस्तृत वर्णन |
| काव्य निर्णय | 1746 | काव्य के भेदोपभेदों का वर्णन |
| श्रृंगार निर्णय | 1750 | नायक नायिका भेद वर्णन |
| विष्णु पुराण भाषा | – | विष्णु पुराण का दोहा-चौपाई शैली में अनुवाद |
| शतरंजशतिका | – | शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन |
| अमर कोश | – | संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद |
पद्माकर
पद्माकर का जन्म बाँदा में 1753 ई. और मृत्यु 1833 ई. में हुआ था। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि, ‘बिहारी रीतिकाल के प्रारम्भिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम।’ पद्माकर जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में में रहे, उन्होंने पद्माकर को ‘कविराज शिरोमणि’ की उपाधि दी। महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने ‘जगद्विनोद’ और ‘पद्मभारण’ की रचना किया। जगत सिंह की मृत्यु के बाद ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी रहे। ग्वालियर में रह कर इन्होंने ‘हितोपदेश’ का अनुवाद किया। इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नांकित हैं-
| ग्रंथ | विषय निरूपण |
| प्रबन्ध काव्य | |
| हिम्मत बहादुर विरुदावली | 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन |
| मुक्तक काव्य | |
| पद्माभरण | अलंकारों तथा नवरसों का विवेचन |
| जगद्विनोद (1811 ई.) | नायक-नायिका भेद, 6 प्रकरण एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन |
| प्रबोधपचासा | भक्ति एवं वैराग्य निरूपण |
| गंगालहरी | संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत ‘गंगा लहरी’ का पद्यानुवाद |
| प्रताप सिंह विरुदावली | 117 छन्दों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन (प्रबंध और चरित काव्य) |
| कलि पच्चीसी | कलियुग का वर्णन |
| राम रसायन | वाल्मीकि के ‘रामायण’ का छायानुवाद |
| अलीजाह प्रकाश | महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है नोट- अलीजाह प्रकाश और जगद्विनोद में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता, कई छंद कुछ शब्दांतर के साथ समान ही हैं। |
पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्यौहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनके काव्य में बुंदेलखण्ड की प्रकृति एवं लोकजीवन का जीवंत चित्रण हुआ है। इनकी भाषा पर बुंदेलखंडी का विशेष प्रभाव पड़ा है।
पद्माकर को हिंदी साहित्य में पचासा शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ ‘जगद्विनोद’ और ‘पद्माभरण’ हैं। इन्होंने ‘जगद्विनोद’ की रचना 1803 से 1821 ई. के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में रहकर किया था। ‘जगद्विनोद’ ग्रंथ में पद्माकर ने श्रृंगार रस के अनुभवों, 8 सात्विक भावों, 12 हावों, 9 रसों, नायक-नायिका भेद, 3 प्रकार के दूतिओं, 4 प्रकार के दर्शन, षड्रऋतुओं आदि का वर्णन किया है। रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ (जगद्विनोद) को श्रृंगार रस का सार मानते हैं।
पद्माकर के ‘जगद्विनोद’ में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। ‘जगद्विनोद’ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की ‘रसमंजरी’, केशवदास की ‘रसिकप्रिया’ और विश्वनाथ प्रसाद के ‘साहित्य दर्पण’ से ली गई है। ‘पद्माभरण’ की रचना इन्होंने जयपुर में किया था, इस ग्रंथ में इन्होंने 100 अलंकारों के लक्षण और उदहारण दिए हैं।पद्माकर के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है की-
1. ‘इनकी भाषा में वह अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदासजी में दिखाई देती है।’
2. ‘ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है।’