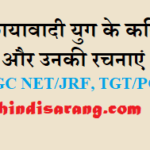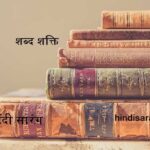काव्य का प्रयोजन
काव्य-प्रयोजन (kavya prayojan) का तात्पर्य है की काव्य रचना का उद्देश्य क्या है? काव्य रचना के उपरांत प्राप्त होने वाला फल क्या है? प्रमुख आचार्यों, विद्वानों, कवियों और आलोचकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के प्रयोजन निम्नलिखित है-
| भरतमुनि | ‘धर्मयशस्यमायुष्यम् हितबुद्धिविवर्धनम्।लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति।।’ |
| भामह | ‘धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्य निषेवणम्।।’ |
| वामन | ‘काव्यं सदृष्टादृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्।’ |
| मम्मट | ‘काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।सद्यः परिनिवृत्तये कान्ता सम्मितयोपदेशयुजे।।’ |
| विश्वनाथ | ‘चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखाल्पधियामपि।काव्यादेवयतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।।’ |
भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन
| आचार्य | काव्य प्रयोजन |
|---|---|
| भरत मुनि | 1.धर्म, 2.यश, 3.आयुष, 4.हित, 5.बुद्धिवृद्धि, 6.लोक उपदेश, 7.दक्षता, 8.चरम विश्रांति प्राप्ति |
| भामह | 1.चतुर्वर्ग फलप्राप्ति 2.कीर्ति, 3.प्रीति, 4.सकल कला-ज्ञान |
| दण्डी | 1.लोक व्युत्पत्ति |
| वामन | 1.कीर्ति, 2.प्रीति |
| रुद्रट | 1.धर्म, 2.कीर्ति, 3.अनर्थोपशम, 4.अर्थ, 5.सुख प्राप्ति |
| आनन्द वर्धन | 1.विनेयन्मुखीकरण, 2.प्रीति |
| कुन्तक | 1.चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, 2.व्यवहार ज्ञान, 3.परमाह्लाद |
| महिम भट्ट | 1.रसमय सदुपदेश, 2.परमाह्लाद |
| अभिनव गुप्त | 1.चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, 2.जायासम्मति उपदेश, 3.परमानन्द, 4.यश |
| भोज | 1.कीर्ति, 2.प्रीति |
| मम्मट | 1.यश प्राप्ति, 2.धन की प्राप्ति, 3.लोक व्यवहार, 4.अनिष्ट का निवारण, 5.आनन्द की प्राप्ति, 6.कान्ता सम्मित उपदेश |
| विश्वनाथ | चतुवर्ग फल प्राप्ति (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) |
आचार्य भरतमुनि ने नाटक के संदर्भ में काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है।
आचार्य मम्मट की दृष्टि काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में समन्वयवादी रही है।
राजशेखर ने कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन किया है।
मध्यकालीन हिंदी साहित्य में काव्य-प्रयोजन
तुलसीदास–
‘स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति।।’
‘कीरति भणिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहंहित होई।।’
‘जस सम्पति, आनन्द अति दुखिन डारै खोई।
होत कवित्त ते चतुराई , जगत् काम बस होई।।’
कुलपति मिश्र
‘जस सम्पति आनन्द अति दुरितन डारे सोई।
होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होइ।।’
देव
‘उँच-नीच अरू कर्म बस, चलो जात संसार।
रहत भाव्य भागवंत जस, नव्य काव्य सुखसार।।’
‘रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप।
जस सरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रुप।।’
सोमनाथ
‘कीरति बित्त बिनोद अरु, अति मंगल को देति।
करै भलौ उपदेश नित, सरस कवित्त चित चेति।।’
भिखारीदास
‘एक लहै तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गुसाई।
एक लहै बहु सम्पत्ति केसव, भूषन ज्यों बरवीर बड़ाई।।’
एकन कों जस ही सो प्रयोजन है, रसखानि रहीम की नाई।।
दास कवितन्ह की चर्चा बुधिवन्तन, को सुख दे सब ठाई।।
सोमनाथ
‘कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देति।
करे भलो उपदेश नित वह कवित्त चित्त चेति।।’
रीतिकालीन हिन्दी आचार्यों ने काव्य-प्रयोजनों के सम्बन्ध में कोई नवीन उद्भावना नहीं की। उन्होंने संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के प्रयोजनों को ध्यान में रखकर काव्य-प्रयोजन निर्धारित किये।
आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन
महावीर प्रसाद द्विवेदी- ‘लेखक का उद्देश्य सदा यही रहा है कि उसके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी हो और साथ ही उसके ज्ञान की सीमा भी बढ़ती रहे।
मैथिलीशरण गुप्त-
‘केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।
उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए।।’
जयशंकर प्रसाद- ‘संसार में काव्य से दो तरह से लाभ पहुँचते हैं- मनोरंजन और शिक्षा।’
रामचन्द्र शुक्ल- ‘काव्य का लक्ष्य है जगत् और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से अपने को निकालकर उसे विश्वव्यापिनी और त्रिकालदर्शिनी अनुभूति में लीन करे।’
‘कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य-हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है।’
हजारी प्रसाद द्विवेदी- ‘मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ।’
नगेन्द्र ‘आत्माभिव्यक्ति वह मूल तत्त्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है।’
नन्दुलारे वाजपेयी- ‘वह रचना काव्य नहीं, जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो।’
गुलाब राय- ‘भारतीय दृष्टि से आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व में नहीं, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है।’
पश्चात् काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन
प्लेटो से लेकर आई. ए. रिचर्ड तक अनेक पाश्चात्य मनीषियों ने काव्य प्रयोजन पर अपने विचार प्रकट किये हैं।
प्लेटो- ‘आन्तरिक उदात्तभाव और सौन्दर्य को उद्घाटित करना, लोक-व्यवस्था और न्याय-संगतता का परिपालन करना, और जगत् के सत्य-रूप की ही अभिव्यक्ति करना।
अरस्तू- ‘कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, पर यह आनंद नीति-सापेक्ष है- यह अनैतिक नहीं हो सकता।’
रस्किन– ‘काव्य का ध्येय है अधिक से अधिक जनसमुदाय की अधिक से अधिक हित-साधना।’
टॉलस्टॉय- ‘यह कला आनंद नहीं है, वरन् मानव-एकता का साधन है, जो मानव-मानव को सह-अनुभूति द्वारा परस्पर संबधित करती है।’
लोंजाइनस- ‘काव्य का एक मात्र लक्ष्य है- पाठक को मात्र आनंद प्रदान करना-उसे बस उल्लसित कर देना।’
स्विनबर्ग- ‘कला का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक मूल्यों का आधार ठीक नहीं है-यह अनावश्यक है।’
ब्रडेले- ‘कला कला के लिए।’, ‘काव्य काव्य के लिए’, ‘काव्यास्वाद अपना लक्ष्य स्वयं है। इसका अपना मूल्य है।’
ड्राइडन- ‘काव्य का प्रयोजन है- मधुर रीति से शिक्षा देना।’
कालरिज- ‘कवि अपने पाठक को नीति का उपदेश देता है, पर इस उद्देश्य का प्राथमिक माध्यम है आनंद।’
वर्ड्सवर्थ- ‘काव्य का लक्ष्य है- सत्य और सौन्दर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना।’
शैले- ‘काव्य जीवन का प्रतिविम्ब है जो इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है।’
मैथ्यू आर्नल्ड- ‘नीति के प्रति विरोध जीवन के प्रति विरोध है।’
आई.ए.रिचर्ड्स- ‘कला कला के लिए सिद्वांत को अस्वीकृत करते हुए काव्य के लिए नैतिकता तथा लोकमंगल को आवश्यक माना।’